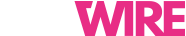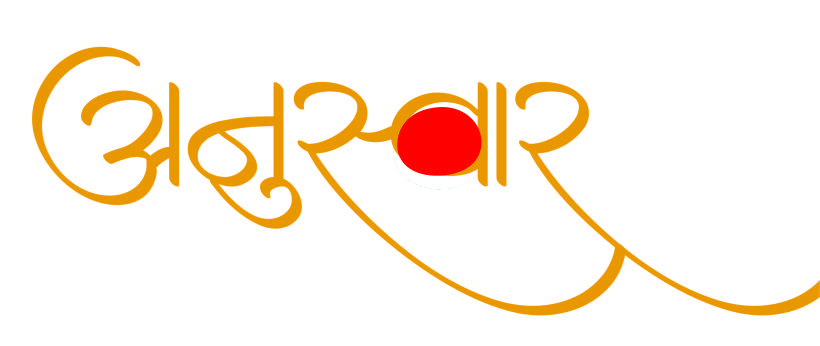सेतु के आर.पार नाटक का संदर्भ विभिन्न भाषाओं, साहित्य और संस्कृतियों के बीच अनुवाद एक सेतु है।श्
प्रो. सुरेश सिंहल
अनुवाद जगत में सन्तोष खन्ना एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रख्यात हो। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें अनुवाद विषय कई प्रकार से घुल.मिल गया है। रच बस गया है और जिसे एक अनुवादमय व्यक्तित्व की संज्ञा दी जा सकती है। काफी लंबे समय से सन्तोष खन्ना भारतीय अनुवाद परिषद् से जुड़ कर अनुवाद के प्रति समर्पित भाव से कार्य करती आ रही हो। यूं तो अनुवाद का कोई ऐसा पक्ष नह° है जिस पर उन्होंने लेखनी न चलाई हो, किंतु उनके द्वारा लिखित अनुवाद विधा पर आधारित ष्सेतु के आर पारष्, शीर्षक से नाटक का प्रकाशन एक सुखद आश्चर्य कहा जा सकता है, क्योंकि अनुवाद विधा को कथ्य बना कर लिखा जाने वाला यह अपने किस्म का प्रथम नाटक है। अतरू अनुवाद के क्षेझ में यह अनुवाद नाटक स्वागत के योग्य है, चूंकि अनुवाद विधा सर्वदा भाषाओं, साहित्य और संस्कृतियों के बीच सेतु का सार्थक साधन रही है इसलिए नाटक का शीर्षक सार्थक बन पड़ा है।
आज के युग में अनुवाद के बढ़ते महत्व को देखते हुए लेखिका ने अनुवाद के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत नाटक का आधार और कथ्य बनाया है। इस नाटक का उद्देश्य अनुवाद विधा से जुड़े प्रश्नों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है।
प्रस्तुत नाटक अनुवाद के क्षेझा में सर्वथा एक नया प्रयोग ही माना जाएगा। निरूसंदेह, नाटक के कलेवर में अनुवाद के विभिन्न पक्षों को समेटना अपने आप में एक कठिन कार्य है। इस संदर्भ में रंगमंच की दृष्टि से अनुवाद को संरचनात्मक स्वरूप प्रदान करना एक सराहनीय कार्य है। अनुवाद को सारे नाटक के कथानक का आधार बनाना, विभिन्न पक्षों की भिन्न.भिन्न पाझाों के माध्यम से चर्चा.परिचर्चा करवाना, संवादों को अनुवाद के वाद.विवाद के रूप में बुलवाना आदि विशेषताएँ प्रस्तुत नाटक को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी हो। उनका यह नाटक नव्यता लिए है और अनुवाद के क्षेझा में ऐसा प्रयास वस्तुतरू सराहनीय और वंदनीय है।
अनुवाद विधा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को इस नाटक में सरस, चुटीले, व्यंग्य और हास्य रस पूर्ण संवादों से ऐसे सजाया गया है कि नाटक बहुत रोचक बन पड़ा है। वास्तव में नाटक अनुवादकों पर समय.समय पर लगे आरोपों के आधार पर आरंभ होता है और नरक में चिझागुप्त न्यायाधीश के रूप में इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे होते हो और जब वह अपने समक्ष आरोपी के रूप में लाये गये अनुवादकों से अनुवाद के बारे में प्रश्न करते हो, उस संबंध में कथोपकथन की एक बानगी देखिए
चिझागुप्त रू आप अनुवादक हो, इसलिए हम जानना चाहते हो कि अनुवाद क्या है?
अनुक 1 रू महाराज, एक भाषा की रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को अनुवाद कहते हो।
यमदूत 2 रू अनुक महोदय, यह अनुवाद की परिभाषा है या उसकी दुम। इतने गंभीर आरोप और इतना संक्षिप्त उत्तर। आप अंगूठी से थान निकालना चाहते हो?
यमदूत 3 रू हरहराती गंगा के सामने बरसाती नाला ।
अनुक 1 रू महाराज, धृष्टता क्षमा हो, आपकी आज्ञा हो तो इसे गोमुख से गंगासागर तक का कर दूँ।
चिझागुप्त रू नह°…नह°। जितना संगत है, केवल उतना ही।
नाटक के प्रथम अंक में अनुवाद की मूल प्रकृति, उसके स्वभाव और स्वरूप को लेकर अनेक प्रश्न सामने आते हो। इनम से अधिकतर प्रश्न अनुवाद विषय पर लगाए जाने वाले आरोपों और आपत्तियों के रूप में आए हो। अनुवाद के साथ.साथ अनुवादक भी इस दायरे में आता है। सबसे पहले अनुवादक पर आरोपों की बौछार होती है ष्अनुवादक को एक सफल साहित्यकार नह° कहा जा सकताष्, मूल आक्षेप के रूप में सामने आता है। इसी संदर्भ में उस पर ष्प्रवंचकष् (पृष्ठ 7), पोंगापंथी (पृष्ठ 8), ष्मूलघातीष् ष्सौंदर्यघातीष्, ष्साहित्यघातीष् (पृष्ठ 8) ष्मिट्टी के शेरष् (पृष्ठ 9) ष्तांझिाकष् (पृष्ठ 11), ष्जादूगरष् (पृष्ठ 12) होने के आरोप मढ़े गए हो।
इसी प्रकार, अनुवाद को भी असंभव करार दे दिया गया है। डॉक्टर जॉनसन के कथन, ष्काव्य का अनुवाद हो ही नह° सकताष्, विक्टर ह्य ूगो के मत, ष्पद्यमय अनुवाद असंभव हैष् और क्रोंचे के विचार ष्अनुवाद उस नारी के समान है जो यदि सुंदर होती है तो वफ़ादार नह° होती और वफ़ादार होती है तो सुंदर नह° होतीष् (पृष्ठ 8) पुष्टि के हेतु दर्शाया गया है। यमदूतों, ष्महादूतष् और स्वयं चिझागुप्त के द्वारा तैयार किए गए इस आरोप पझा का सटीक एवं न्यायोचित उचित उत्तर अंक पांच में चिझागुप्त के माध्यम से उनके निर्णय के रूप में इस प्रकार दिया गया है
ष्अनुवादक न तो प्रवंचक है और न ही जादूगर है और न ही किसी और की प्रतिभा के आधार पर मौज.मस्ती या गुरछर्रे उड़ाने वाला कोई व्यक्ति है। अनुवादक वस्तुतरू परहितकारी एवं समन्वयकारी एक ऐसा मनीषी है जो अपने परिश्रम, लगन, त्याग, तपस्या एवं मूल के प्रति निष्ठा से भाषा.भाषा के बीच की दूरियाँ मिटाता है, भिन्न.भिन्न काल खंडों को समीप ले आता है। भिन्न.भिन्न साहित्यों में परिचय करता है।
लोकहित का यह कार्य अनुवादक को दिया गया है। सच्चा और पारंगत अनुवादक कोई मामूली व्यक्तित्व नह°, अपितु उसकी गरिमा ईश्वर आराधक से भी कह° अधिक है। वह केवल भाषाओं के बीच सेतु का साधन नहीं, बल्कि संस्कृतियों के बीच संपर्क स्थापित करता है। ऐसा प्राणी वस्तुतरू वंदनीय है, मो अनुवादक को हर प्रकार के आरोप से बरी करता हूँ। (पृष्ठ 116.17)
इसी प्रकार, अनुवाद विषय पर लगाए गए सभी आरोपों को भी न्यायाधीश चिझागुप्त के द्वारा ख़ारिज किया गया है, श्अनुवाद मानव और मानव के बीच संवाद है, विभिन्न संस्कृतियों के विविध रूपों की झांकियों को प्रदर्शित करने का एक स्वच्छ दर्पण है, मानव मनीषा के नए.नए विचारों का कोषागार है। कम से कम वर्तमान युग में कोई भी आयाम अनुवाद से अधिक मानव मिझा हो ही नही° सकता जब किसी साहित्यिक रचना का अनुवाद होता है तो अनुवाद केवल भाषा के स्तर पर ही नही° होता है अपितु वह भाषा, विचार, संस्कृति, इतिहास आदि के स्तर पर भी होता है। अनुवाद के माध्यम से श्रोत भाषा की संपूर्ण साहित्यिक परंपरा लक्ष्य भाषा में उपस्थित हो जाती है और लक्ष्य भाषा के रचनाकार साहित्य, समाज एवं संस्कृति को एक नए रूप में प्रमाणित करती है। (पृष्ठ 116)
निरूसंदेह, चिझागुप्त के माध्यम से उसके निर्णय के रूप में अनुवादक और अनुवाद विधा पर सभी आरोपों और भ्रांतियों को लेखिका ने बखूबी ख़ारिज करते हुए अनुवाद को एक स्वतंझा साहित्यिक और महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित करने का संदेश दे कर इस नाटक की सार्थकता को सिद्ध किया है।
नाटक के अंक दो में लेखिका ने अनुवाद की परिभाषा, अर्थ, विकास, प्रक्रिया, प्रकार, स्वरूप आदि जैसे विभिन्न आयामों को समाहित किया है। इस दृष्टि से नाटक का यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम, चिझागुप्त अनुवाद की अवधारणा को लेकर अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हो। इसके उत्तर में कहा गया है कि ष्विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और समृद्धतम भाषा संस्कृत में अनुवाद शब्द विराजमान है। इस शब्द की व्युत्पत्ति ष्अनष् (उपसर्ग), ष्वदष् धातु, ष्घसाष् (प्रत्यय) से हुई है जिसका शब्दार्थ है किसी कथन के बाद उसे दुहराना। आरंभ में अनुवाद का अर्थ विधिप्राप्तस्य वाक्यांतरेण कथने ष्अर्थात् विधायक शास्झा द्वारा कही गई बात को वाक्यांतर में पुनरू कहना था। अनुवाद शब्द का ऋग्वेद में भी उल्लेख हैरू ष्अन्वेको न् वदति यद्दाति।ष् यहाँ ष्अनुष् और ष्वदतिष् का अर्थ दुहराना है। बृहदारण्यक उपनिषद् में ष्तद्, तद्, वैशा देवी वाग् अनुवदतिष् में अनुवदति का प्रयोग दुहराने के अर्थ में हुआ है।
यमदूत 1 रू अनुक महोदय संस्कृत साहित्य का उल्लेख कर रहे हो तो बताइए क्या संस्कृत के शीर्षस्थ विद्वान पाणिनि के मानक मूल व्याकरण ग्रंथ ष्अष्टाध्यायीष् में ष्अनुवादष् शब्द का उल्लेख हुआ है।
अनुक 1 रू जी हाँ, उसम ष्अनुवाद चरणामृष् में अनुवाद स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक भाषा के रूप काव्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना, जैसे काव्य को गद्य में उतारना आदि।
आज विद्वान इसे ष्इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशनष् भी कहते हो। संस्कृत अध्यापन में एक प्रकार से अनुवाद का प्रयोग होता था जो आज भी विद्यमान है। (पृष्ठ 15) इस प्रकार लेखिका ने नाटक म अनुवादक पाझाों के द्वारा अनुवाद के प्रारंभिक अर्थ को स्पष्ट करने के बाद उसके स्वरूप को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अनुवादक पाझाों में से एक अनुवादक पाझा कहता है कि अनुवाद अत्यंत दुष्कर कार्य है मौलिक लेखन से भी कठिन। (पृष्ठ 19) ये नट की रस्सी पर चलने की कला है (पृष्ठ 19) अनुवाद के इस सिद्धांत के स्वरूप को सिद्धांतकार नामक पाझा के कथन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है
ष्अनुवाद अन्य कलाओं की भांति एक रचनात्मक विधा है। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद एक कलात्मक प्रक्रिया है। अनुवाद को मूल रचनाकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर मौलिक सृजन की भांति विचार, भाव और भाषा में लालित्य और चमत्कार का समावेश करना पड़ता है। यही नहीं, मूल रचना में निहित बिंब, प्रतीक और अभिप्राय तथा इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचनात्मकता की आंतरिक लय को रूपांतरित करना होता है।
अनुवाद प्रक्रिया में मूल रचना के मूल स्वर को अंतरित करते समय अनुवादक को आत्म साक्षात्कार द्वारा मूल रचनाकार के मानस म प्रवेश करना पड़ता है इसलिए अनुवाद को परकाया प्रवेश की संज्ञा दी गई है। अनुवाद तप है, कठिन साधना है कोई यंझा.तंझा नह° जैसा कि अनुवादक पर आरोप है। महाराज, अनुवाद एक सुंदर पुष्प की सुगंध को दूसरे सुंदर पुष्प की सुगंध में उड़ेलने की कला है एवं यह अत्यंत सूक्ष्म एवं जटिल प्रक्रिया है। (पृष्ठ 21) जब तक इस कार्य में ष्स्वष् का पूर्ण विसर्जन नह° हो जाता, अनुवाद असंभव है। (पृष्ठ 25) अनुवाद सदैव इस बात को लेकर विवाद का विषय रहा है कि क्या यह कला है, शिल्प है या फिर विज्ञान है। इस विषय में भी प्रस्तुत नाटक में सार्थक स्पष्टीकरण दिया गया है। सिद्धांतकार का कथन यहाँ प्रासंगिक है ष्अनुवाद कार्य केवल कला नह° कला, शिल्प और विज्ञान का संगम है।
अनुवाद के शिल्प होने के दो पक्ष हो। पहला, पहले साधारणतया अनुवाद श्रेण्य ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और प्रेरक साहित्य का किया जाता था। अनुवादक ऐसे अनुवाद धीरे.धीरे यथा क्षमता सुंदर, अलंकृत और दार्शनिक शैली में करते थे। अब अनुवाद का क्षेझा अत्यंत विस्तृत है। विभिन्न भाषा.भाषियों के विचारों, भावों एवं विभिन्न उपलब्धियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर दी गई है। वस्तु साहित्य का सामान्यतया एक निश्चित समय सीमा में सीधी.सादी नपी.तुली और अलंकार रहित शैली में बोधगम्य अनुवाद करना होता है। सामान्य अर्थ में अनुवाद कार्य करने की कुशलता ही शिल्प है।
दूसरा, अपने व्यापक रूप में शिल्प का अर्थ है भाषा प्रयोग, संरचनात्मक बोध और वाक्य विन्यास। अनुवाद में इसकी भूमिका साधन की है। कला साध्य है तो शिल्प साधन है। इस साधन के प्रयोग की विधि ही विज्ञान है (पृष्ठ 25)। यह विज्ञान इसलिए भी है, क्योंकि यह अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है तथा अनुवाद से पहले की चिंतन प्रक्रिया तुलनात्मक या व्यतिरेकी भाषा विज्ञान पर ही पूर्णतया आधृत है। (पृष्ठ 30) अनुवाद की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है इसको लेकर भी प्रस्तुत नाटक में साहित्यकार पाझा द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि क्या अनुवादक भी मूल रचनाकार की भांति साहित्य.सर्जन जैसी ही प्रक्रिया से गुजरता है। इस संदर्भ म दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं साहित्य और अनुवाद की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है
रचना प्रक्रिया में कवि अर्थात् साहित्यकार जब विषय विशेष के प्रति संवेदनशील होता है और उस स्वरूप में जिस भाव राशि का विस्फोट होता है तो उसकी प्रतिक्रिया में अभिव्यक्ति के लिए वह आतुर हो उठता है तब वह भाव भाषा रज्जू के सहारे आकार लेने लगते हो। इस प्रक्रिया के दौरान वह उन भावों म से सीप सा चयन करता है और एक स्वतंझा रचना करता है। काव्य.सृजन मन में उठने वाले भावों का अनुवाद है जो संवेदना की अनुभूति पर आधारित होते हो। (पृष्ठ 27)
इस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया में भी लगभग यही सोपान होते हो। मूल रचना को पढ़ने से अनुवादक के मन म संवेदनाजनित अनुभूति के आधार पर भाव प्रस्फुटन होगा। मूल रचनाकार के मन में किसी विषय एवं स्थिति विशेष के प्रति प्रक्रिया स्वरूप भाव स्फुटन होता है। साहित्यकार के लिए भावों को भाषाबद्ध करते समय कोई सीमा नह° होती जबकि अनुवादक के लिए सीमा होती है।
वह मूल भाषा में व्यक्त भावों को ही लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करता है तभी तो मेंको पुनरू सृजन के नाम से अभिहित किया गया है। (पृष्ठ 28) सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में कविता के अनुवाद की समस्याएँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। प्रस्तुत नाटक में भी लेखिका ने अनेक ऐसी समस्याओं पर विचार किया है और उनका प्रामाणिक और विज्ञान.सम्मत समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। यहाँ इन समस्याओं को विभिन्न आक्षेपों के रूप में दर्शाया गया है। ष्काव्य मानव की उदात्त और अद्वितीय अनुभूतियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है और काव्य अनुवाद की प्रक्रिया में यह उदात्त एवं अद्वितीय अनुभूतियाँ औसत अनुभूतियों में परिणत हो जाती हो (पृष्ठ 55.56) या ष्फिर अनुवाद में रचना अपने मूल से बहुत दूर हो जाती है। (पृष्ठ 56) ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए प्लेटो के कथन, ष्कवि जीवन की ऐसी अनुकृति करता है जो यथार्थ से दुगनी दूर होती है (पृष्ठ 56) अरस्तु के कथनµ पε चवमज पे उंकेए पज पे कपअपदम उंकदमेण् और रविंद्रनाथ टैगोर के कथन, ष्अनूदित कविता पढ़ना किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन लेने के समान है।
अनुवादकों पर एक यह आरोप भी लगाया गया है कि असफल लेखक ही काव्यानुवाद की ओर प्रवृत्त होते हो। (पृष्ठ 78) इसके उत्तर में लेखिका ने एक अनुवादक पाझा से यह संदेश दिया है कि ऐसा होता तो भारतदु हरिश्चंद्र, रविंद्र नाथ टैगोर, महावीर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन आदि प्रतिष्ठित एवं स्थापित सफल साहित्यकार अनुवाद करते।… रव°द्रनाथ टैगोर उच्च कोटि के अनुवादक थे। उन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी में स्वयं अनुवाद किया और इसी अनुवाद पर उन्ह नोबेल पुरस्कार मिलता है। (पृष्ठ 78) इसी क्रम में काव्यानुवाद की कुछ और समस्याएँ और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम, अनुवादक का काव्यानुवाद में छूट लेना कहाँ तक उचित है? प्रश्न के उत्तर में सिद्धांतकार पाझा कहते हो कि कवि के चेतन.अवचेतन से जो भाव अभिव्यक्ति के लिए मचल रहे होते हो उन्ह भाषा की पकड़ में लाना भी कठिन होता है।
आकार लेते.लेते उसम से कुछ छूट जाता है जिसे ष्मन के पुष्पक क्षणों की आधी पंखुड़ियाँ का गिरनाष् कहा गया है, इसी प्रकार, काव्यानुवाद के दौरान कुछ और जुड़ भी जाता है, किंतु यदि कुछ और कविता के मूल अर्थ को प्रभावित किए बिना आए तो इसे दोष नह° माना जाना चाहिए। (पृष्ठ 79.80) एक अन्य प्रश्न, ष्काव्यानुवाद में अनुवादक को कौन.सा रास्ता अपनाना चाहिए के उत्तर में कहा गया है किष् अनुवादक को सर्वप्रथम श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच समानार्थकता की खोज करनी चाहिए। अनुवाद एक व्याख्यापरक कला है।
7अनुवादक को श्रोत भाषा की मानसिक धरातल पर व्याख्या कर उसके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। व्याख्या के दौरान अर्थ प्रकाश से कवि का अर्जित अनुभव अनुवादक का अर्जित अनुभव हो जाता है और फिर उसे आवश्यकता होती है लक्ष्य भाषा में श्रोत भाषा की शैली की, तभी वह पुनरू सृजन कर सकता है। (पृष्ठ 80) इसी कड़ी में अगली समस्या, ष्क्या अनुवादक को मूल रचनाकार की शैली का अनुसरण करना चाहिएष् के उत्तर में लेखिका कहती हो कि ष्प्रत्येक रचना के दो भाग होते हो शिल्प और शैली। शिल्प भंगिमा विशेष को कहते हो। अनुवादक को मूलनिष्ठ अनुवाद करने के लिए मूल रचनाकार की शैली का ही अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करने में शब्द, ध्वनि, रूप आदि पर समस्याएँ उठ सकती हो।
अप्रस्तुत विधान, बिंब, अलंकार आदि का अनुवाद भी अपेक्षित है।ष् (पृष्ठ 80) ष्कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्या अप्रस्तुत विधान को प्रस्तुत किया जा सकता हैष् जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में सिद्धांतकार पाझा कहता है कि ष्अप्रस्तुत का अंतरण न करने से कविता की रचनात्मकता की क्षति होती है। सामान्यतया ऐसी अभिव्यक्तियों का अनुवाद संभव होता है किंतु अनेक बार संस्कृतियों एवं पौराणिक संदर्भ से युक्त समान धर्म व्यंजनाएँ ढूँढ पाना असंभव होता है। ऐसी स्थिति में पाद टिप्पणी अथवा कोष्ठक में व्याख्या दे देनी चाहिए।ष्
दार्शनिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अनुवाद की समस्या के संदर्भ म कहा गया है कि ऐसा नह° है कि इनका अनुवाद संभव न हो इस के लिए अनुवादक को उतना ही कल्पना.प्रवण और संवेदनशील होना होता है जितना मूल कवि। जब मूल म व्यक्त अभिव्यक्ति के समतुल्य अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा म नह° मिलती तो उसी प्रकार का भाव व्यक्त करने वाली अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ( पृष्ठ 82.83)
साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में नाटकानुवाद भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। प्रस्तुत नाटक में लेखिका ने नाटकानुवाद की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। नाटकानुवाद की कुछ समस्याओं का शेक्सपियर को केंद्र में रखकर चिझाण किया गया है। शेक्सपियर के नाटकों के अनुवादकों ने अनुवाद किए हो, किंतु समय.समय पर उन पर कोई न कोई आरोप लगता ही रहा है। मूल रूप से नाटकों के अनुवाद के बारे में यह आरोप लगा है कि अनुवादकों ने अनुवाद के नाम पर नाटकों को ऐसा तोड़ा.मरोड़ा है कि उनकी पहचान ही समाप्त हो गई है। ना तो वह अपने ष्जनकष् के ही रहे और न ही ष्जानकीष् बन पाए। (पृष्ठ 60) एक तरह से कहा जाए तो शेक्सपियर के नाटकों का जनाजा निकाला गया। यह अनुवाद मूलनिष्ठ बिल्कुल नह° थे यहाँ तक कि उन्ह उन नाटकों की छाया तक कहने में संकोच होता है। उदाहरण के लिए, लाला संतराम का अनुवाद किलष्ट है, रांगेय राघव का अनुवाद पैराफ्रेज जैसा है और उन्होंने मूल के कई अंश का अनुवाद किया ही नह° है और भारतदु ने पाझाों के नामों का भारतीयकरण कर दिया है। (पृष्ठ 62.62) अन्य अनुवादकों ने भी अपने ढंग से किसी एक नाटक की कहानी ली और उसे विजातीय संस्कृति में ढाल दिया।
उन्होंने अपनी ओर से उनम गीतों की भरमार कर दी और कहानी को मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा। (पृष्ठ 62.64) इसी कारण शेक्सपियर अभी भी अपनी संपूर्णता के साथ अनुवाद में नह° आ पाए हो। जिन्होंने शेक्सपियर के मूल नाटकों को पढ़ा है वह अनुवाद के ष्बौनेपनष् से परिचित हो। उनम कविता नदारद है सपाट और शुष्क। (पृष्ठ 64) और रस निष्पत्ति भी देखने को नह° मिलती। (पृष्ठ 65) एक विद्वान ने कहा हैµ शेक्सपियर के अब तक के अनुवादों में उसका चोला जी सका, आत्मा नह°। (पृष्ठ 67) उक्त सभी आरोपों और समस्याओं की बहुपक्षीय सफाई एवं समाधान सूझा प्रस्तुत किए गए हो।
हमारे यहाँ शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद की परंपरा एक सदी से भी अधिक पुरानी है। आरंभ में उनके अनेक नाटकों का मुक्तानुवाद हुआ, इन अनुवादों की अनेक रंगमंच प्रस्तुतियाँ हुईं जो जनसाधारण में बेहद लोकप्रिय हुई। यह कार्य अनुवादकों ने किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नह° किया।
वे तो पाठकों/दर्शकों को इस महान लेखक से परिचित कराना चाहते थे/अनुवादकों ने तो शेक्सपियर को अपने अनुवाद के द्वारा विभिन्न भाषाओं में ष्अमरष् किया है। इन लोगों का उद्देश्य मूल भाषा से अनभिज्ञ पाठकों को मूल कृति से परिचित कराना रहा है। भारतदु हरिश्चंद्र ने भी यही सोच कर शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया। वे अनुवाद करने में मूल.भाव को ज्यों.का.त्यों ग्रहण करने में समर्थ थे किंतु साथ ही अनूदित कृति पर अपने देश, भाषा, संस्कृति की मौलिक छाप छोड़ने के पक्षधर थे।
अतरू उन्होंने ष्मर्चेंट ऑफ वेनिसष् का भारतीयकरण किया। अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय ने भी अनेक नाटकों का अच्छा अनुवाद किया है। बच्चन ने शेक्सपियर की चार महान झाासदियों और रघुवीर सहाय ने ष्मैकबेथष् का पद्य अनुवाद किया है। यह सभी अनुवाद परवर्ती अनुवादों से वस्तुतरू बेहतर हैं।
इन अनुवादों में इस समय की मांग के अनुसार ऐसे प्रसंग भी सम्मिलित कर लेते थे जो जन जागृति में सहायक होते थे। दरअसल, नाटकानुवाद काव्यानुवाद से भी कठिन कार्य है। इसम काव्य बिंब के साथ नाट्य बिंब का भी अनुवाद करना होता है। उसम प्रयुक्त संवाद की संश्लिष्टता होती है उसम एक.सा स्वर नह° होता। कह° गंभीर, कहीं, व्यंग्यात्मक, कह° हास्यात्मक संवादों की विविध प्रकार की छटा को अनुवाद में उतरना होता है। यह सब अनुवादकों की बदौलत ही संभव हो पाया है।
सन्तोष खन्ना का नाटक ष्सेतु के आर पारष् अपने आप में एक नया प्रयोग है ही, अनुवाद की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अनुवाद विषय को सरल एवं रोचक ढंग से समझने समझाने के लिए यदि इसका मंचन किया जाए तो यह सभी अनुवादप्रेमियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रस्तुत नाटक की समीक्षा इस उद्देश्य से की गई है कि यह एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक शोध लेख के रूप में शोधार्थियों/विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। निश्चित ही प्रस्तुत अनुवाद नाटक का अनुवाद जगत म अनुवाद प्रेमियों के द्वारा स्वागत किया जाएगा।
यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि लेखिका का एक और नाटक ष्तुम कहो तोष् एक सामाजिक नाटक है जिसम उन्होंने समाज की समस्याओं को उठाया है। इसके अलावा, लेखिका ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार बर्नार्ड शॉ के नाटक ष्सट जोनष् का हिंदी में नाट्यानुवाद भी किया है। इस अनूदित नाटक का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा मंचन किया जा चुका है।
ष्ननकू के जूतेष् शीर्षक से एक एकांकी नाटककार सन्तोष खन्ना ने बच्चों के लिए लिखा था जिसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की बाल पझिाका ष्बाल भारतीष् में प्रकाशित किया गया था।